देह-दान (शरीर दान)
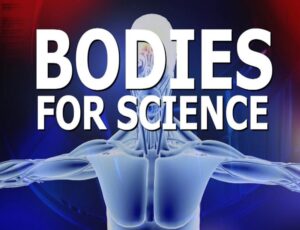
देह–दान क्या हैं?
देह दान के विषय में अनेक भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। इसकी सही जानकारी होना जरूरी हैं। जब कोई व्यक्ति मेड़िकल अध्ययन के लिए अपना शरीर दान देता हैं तो उसे देह-दान कहा जाता हैं। मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थीयों के लिये शरीर का ज्ञान आवश्यक होता हैं। विद्यार्थीयों को अभ्यास में इन शरीरों से मदद मिलती हैं और वे भविष्य में मानव शरीर संरचना को सही रूप में समझ कर मरीजों पर कठीन सर्जरी और रोग का निदान कर सकते हैं।
यह दान अधिकृत मेडिकल कॉलेजों के एनाटॉमी विभाग में संभव है। कॉलेज एक अन्य अस्पताल से भी जुड़ा हो सकता है (जिसमें अत्यधिक विशिष्ट कौशल और आवश्यक सहायक सेवाओं द्वारा चिकित्सा देखभाल प्रदान करने की एक विशेष सुविधा हो) या एक शिक्षण अस्पताल जहां इसका उपयोग केवल छात्रों के अनुसंधान या प्रशिक्षण के उद्देश्य से किया जाएगा।
स्वैच्छिक देह–दान के लिए एनाटॉमी अधिनियम
शरीर दान के लिए एनाटॉमी अधिनियम 1948 में, एनाटॉमी अधिनियम भारत के सभी राज्यों में पारित किया गया था। यह सरकार को अनुमति देता है कि निर्धारित समय – सीमा 48 घंटे के भीतर, यदि किसी के शरीर पर कोई दावा नहीं किया जाता है तो उसे अनुसंधान उपयोग के लिये दे सकती हैं।
महाराष्ट्र एनाटॉमी एक्ट, 1949 भारत में अधिनियमित पहला अधिनियम था – “यह अधिनियम अस्पतालों और चिकित्सा और शिक्षण संस्थानों को मृत व्यक्तियों (या दान किए गए शरीर या मृतक व्यक्तियों के किसी भी हिस्से) को शारीरिक परीक्षा और विच्छेदन और अन्य समान उद्देश्यों के लिए स्वीकार करने की अनुमति देता हैं।
देह–दान कैसे किया जाता हैं?
- मृत्यु से पहले, नजदीकी मेडिकल कॉलेज से संपर्क करके, देह-दान का फॉर्म भरें और इसे अस्पताल के शरीर रचना विभाग (Anatomy Dept.) के प्रमुख के पास जमा करें।
- घर पर या अस्पताल में मृत्यु होने के बाद, परिवार वाले दान दाता की इच्छानुसार प्रार्थना कर के देह अस्पताल के शरीर रचना विभाग को सौंप देवें।
- घर पर मृत्यु होने के आधे घंटे के भीतर अस्पताल को सूचित करें ताकी उन्हें सारी व्यवस्था करने का समय मिल सके।
- हमारा देश गर्म हैं, इसलिये मृतक को ठंड़ी मशीन वाले ताबूत (फ्रीजर में आठ घंटे तक रख सकते हैं) रखें।
- टी.बी., कैंसर, एच.आई. वी, कोविड और चिकित्सकीय कानूनी मामले (मेडिको लीगल केस-ख़ुदकुशी, हत्या आदि ) या किसी संक्रामक रोग से पीड़ित मरीजों का देह दान नहीं हो सकता।
देह–दान का उद्देश्य
- देह मानव शरीर को समझने और विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए उपयोगी हैं।
- विच्छेदन द्वारा चिकित्सा छात्रों को मानव शारीरिक संरचनाओं और साइकोमोटर कौशल के विकास के संबंधों को सीखने में मदद मिलती है। यह माध्यम किसी भी पाठ्यपुस्तक या कंप्यूटर से भी अधिक व्यावहारिक चिकित्सा ज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत है।
- सर्जनों और अन्य लोगों को शरीर-रचना प्रयोगशाला (कैडेवर लैब), कार्यशालाओं में नवीन सर्जिकल कौशल और प्रक्रियाओं का प्रयोग करने में मदद करता हैं।
देह-दान के विषय में भ्रांतियाँ:
1.भ्रांति: अंगों को मृत व्यक्ति से निकाल कर प्रत्यारोपण के लिए वितरित किया जाएगा:
सच: नहीं यह सच नहीं हैं। घर या अस्पताल में मरने वाले व्यक्ति के अंगों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। केवल नियंत्रित स्थिति में ही ब्रेन-स्टेम मृत व्यक्ति से प्राप्त अंगों को प्रत्यारोपण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- भ्रांति:सभी निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्वैच्छिक शरीर दान स्वीकार कर सकते हैं।
सच: निजी मेडिकल कॉलेज केवल एनाटॉमी (शरीर रचना विज्ञान) अधिनियम के अनुसार लावारिस शव ले सकते हैं। ऐसे बहुत कम कॉलेज हैं जिन्हें स्वैच्छिक दान स्वीकार करने की अनुमति मिली हुई है। दान आमतौर पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में किया जाता है।
- भ्रांति:बहु-अंग दान के बाद देह-दान किया जा सकता हैं।
सच: जब बहु-अंग दान के बाद देह-दान नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं होता है। मेडिकल स्कूलों को एक पूर्ण शरीर की आवश्यकता होगी, और आम तौर पर प्रत्यारोपण के लिए अंगों या ऊतकों को हटाने के लिए एक व्यक्ति के शरीर को अस्वीकार कर दिया जाएगा। लेकिन कॉनिया-दान (नेत्रदान) के बाद देहदान संभव है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- कौन अपना शरीर दान कर सकता है?
मृत्यु के बाद लगभग कोई भी संपूर्ण शरीर दाता बन सकता है। ऊपरी आयु सीमा नहीं है। यहां तक कि जो बहुत बीमार हैं वे भी पात्र हो सकते हैं, क्योंकि शोधकर्ताओं को अक्सर उन दाताओं की आवश्यकता होती है जिनके पास एक विशिष्ट बीमारी या चिकित्सा स्थिति होती है।
- क्या देह-दाता बनने के लिए अग्रिम रूप से पंजीकरण करना आवश्यक है?
एक देह-दाता बनने के लिए अग्रिम रूप से पंजीकरण करना आवश्यक नहीं है। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी व्यक्ति की इच्छाओं के बारे में कोई भ्रम नहीं है और समय आने पर सारी अंतिम क्रियायें शीघ्र और सुचारू रूप से पूरी होने के लिये, किसी संगठन या मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग से पहले से जुड़ना उपयोगी हो सकता है।
- देह-दान के लिए पंजीकरण प्रक्रिया क्या है?
निकटतम अस्पताल या मेडिकल कॉलेज या एनजीओ की पहचान करें जो शरीर दान की सुविधा प्रदान कर सकते हैं और पूरे शरीर के पंजीकरण के लिए उनकी आवश्यकताओं को समझने के लिए उनसे संपर्क करें। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नियमों और प्रक्रियाओं का थोड़ी अलग हो सकती है। मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में पंजीकरण फॉर्म और शरीर दान के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। दान की प्रक्रिया को समझने के बाद स्वयं को स्वैच्छिक दान कार्यक्रम के तहत पंजीकृत करें।
मेडिकल कॉलेज देह-दान फॉर्म
आज हर मेडिकल कॉलेज के अपने देह–दान फॉर्म हैं और कई कॉलेजों में तो 20 पन्नो के देह–दान फॉर्म हैं, जो दान दाता को फॉर्म भरने से विमुख कर देते हैं। देह–दान का यह अभियान तभी सफल हो सकेगा, जब पूरी प्रक्रिया सरल हो और एनाटॉमी अधिनियम के अनुसार भारत के सारे मेडिकल कॉलेज के फॉर्म एक समान, छोटे और सटीक हो।